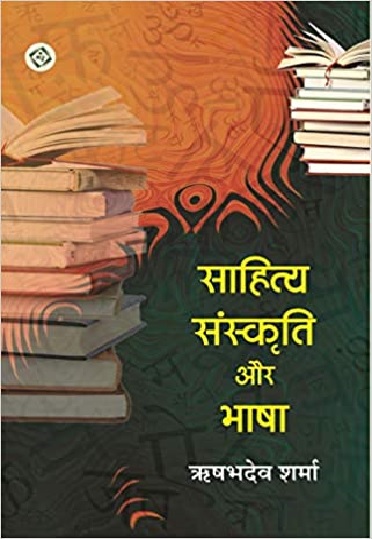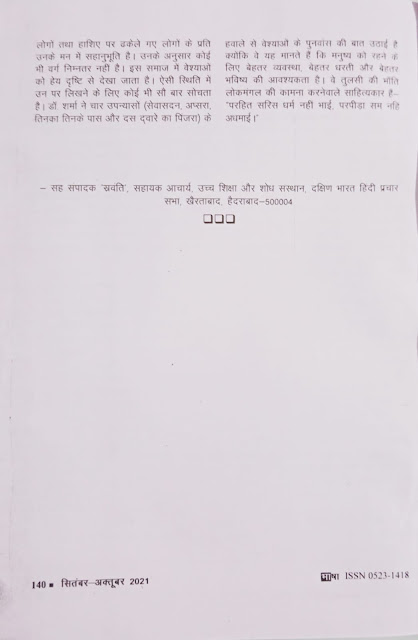- प्रवीण प्रणव
लेखिका गुर्रमकोंडा नीरजा की किताब ‘समकालीन साहित्य विमर्श’, वर्तमान समय के कई ज्वलंत मुद्दे, जो नए नहीं हैं, पर एक नई दृष्टिकोण डालने का प्रयास है। हालांकि लेखिका ने लिखा है कि इस किताब में संकलित लेख 2008 से 2020 के बीच अलग-अलग संदर्भों में लिखे गए हैं लेकिन इससे न तो क्रमबद्धता और न ही पठनीयता प्रभावित होती है। हम सब साक्षी हैं कि कुछ वर्षों पहले जब किसी पुल का निर्माण होता था, महीनों, सालों तक मजदूर काम करते थे और आरंभ से अंत तक पुल का निर्माण वहीं होता था। लेकिन आज पुल बनाने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। पुल के कई भाग अलग-अलग जगहों पर बनते हैं और अंत में उन्हें जहाँ पुल बनना होता है, वहाँ ला कर जोड़ा जाता है। साहित्य की दृष्टि से पहले पुल बनाने की प्रक्रिया को आधुनिक काल कह सकते हैं और वर्तमान तरीके को उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक साहित्य जिसे समकालीन साहित्य भी कहा जाता है, के विभिन्न विमर्शों को जी. नीरजा ने पुल के अलग-अलग भागों की तरह एक साथ ला कर इस तरह जोड़ा है कि इस किताब के स्वरूप में लेख, अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं।
आज के दौर में विमर्शों का बोलबाला है। हर साल-दो साल के बाद कोई नया विमर्श ‘चलन’ में आता है और साहित्यकारों की लेखनी उस विमर्श पर ऐसे-ऐसे लेख लिखती है कि भविष्य में इस विमर्श से जनित किसी भी क्रांति के लिए ‘गंगा की गंगोत्री’ उनके ही लेख को ठहराया जा सके। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर साहित्यकारों की दृष्टि पूर्वाग्रहों से प्रेरित रही है। अज्ञेय ने कहा “अगर मैं मानता भी हूँ कि समाज को बदलने में साहित्य का योग होता है, कि उसमें साहित्यकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो भी आज साहित्यिक रचना और सामाजिक परिवर्तन में जैसा सीधा समीकरण बनाया जा रहा है, उसे मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग 50 वर्षों से इस तरह का सीधा संबंध बनाने और सिद्ध करने का जो एक प्रयत्न होता रहा है, उसने साहित्य का बहुत अहित किया है। आलोचना को, जिसका लोचन से संबंध ही स्पष्ट करता है कि उसे स्वच्छ प्रकाश की अनिवार्य आवश्यकता है, उसने एक धुंधलके में भटका दिया है। रचना की दृष्टि को एक रंगीन चश्मा पहनाकर उसने एकांगी और असमर्थ बना दिया है।“ संतोषप्रद है कि जी. नीरजा साहित्यिक विश्लेषण और विमर्श के लिए किसी रंगीन चश्मे का इस्तेमाल न करते हुए, अपने लेखों के माध्यम से, इन विमर्शों में पूर्व में स्थापित और सत्यापित तथ्यों से इतर कुछ नये आयाम जोड़ती हैं।
इस किताब में 24 लेख हैं जिन्हें पाँच खंडों में संकलित किया गया है। पहला खंड ‘हरित विमर्श’ है। यूं तो इस खंड में सिर्फ दो लेख हैं लेकिन लेखिका इन दो लेखों के माध्यम से पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने में सफल रही हैं। बिहारी सतसई का दोहा “देखन में छोटे लगैं घाव करैं गम्भीर”, इन दोनों लेखों के लिए सटीक बैठता है।
“हरित विमर्श की प्रस्तावना” शीर्षक लेख में लेखिका ने पर्यावरण विमर्श को स्त्री विमर्श के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि “सामान्यतः धरती को स्त्री के समान और स्त्री को धरती के समान माना जाता रहा है। लेकिन अधिकार और सत्ता की अपार इच्छा पुरुषवादी व्यवस्थाओं के चरित्र को शोषण की मनोवृत्ति से संपन्न करती रही है। इस मनोवृत्ति के कारण ही पुरुष केंद्रित समाज का विकास, पर्यावरण और स्त्री के निरंतर दोहन पर टिका है। इस दोहन के पीछे पुरुष की आधिपत्य की भावना है।“ केरल की प्रसिद्ध साहित्यकार के. वनजा भी स्त्री और धरती में समानता की बात करती हैं। दुनिया की प्रकृति पर पितृसत्ता के अधिकार के खिलाफ़ स्त्री एवं प्रकृति केंद्रित इको फेमिनिज्म की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। के. वनजा ने अपने तीन किताबों की शृंखला - “साहित्य का पारिस्थितिक दर्शन”, “इकोफेमिनिज्म”, और “हरित भाषा वैज्ञानिक विमर्श” में इस विषय पर महत्वपूर्ण काम किया है।
“पर्यावरण के प्रश्न और कविता” शीर्षक लेख में लेखिका ने समकालीन कवियों की कविताओं के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की बात की है। प्रो. ऋषभदेव शर्मा की कविता की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लेखिका सशंकित हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की तरफ हम इतनी दूर आ गए हैं जहाँ से वापसी का रास्ता सरल नहीं। "हैलो, मनुष्य,/ मैं आकाश हूँ। /कल सृजन था, निर्माण था,/ आज प्रलय हूँ, विनाश हूँ।/ मेरी छाती में जो छेद हो गए हैं काले काले,/ ये तुम्हारे भालों के घाव हैं,/ ये कभी नहीं भरने वाले।"
पेड़ों की कटाई और कंक्रीट के जंगल बसाए जाने से संभावित खतरों की बात करते हुए लेखिका, कविता वाचक्नवी की कविता उद्धृत करती हैं "मेरे हृदय की कोमलता को / अपने क्रूर हाथों से / बेध कर / ऊँची अट्टालिकाओं का निर्माण किया/ उखाड़ कर प्राणवाही पेड़-पौधे/ बो दिए धुआँ उगलते कल - कारखाने / उत्पादन के सामान सजाए / मेरे पोर-पोर को बींध कर / स्तंभ गाड़े / विद्युत्वाही तारों के / जलवाही धाराओं को बाँध दिया। / तुम्हारी कुदालों, खुरपियों, फावडों, / मशीनों, आरियों, बुलडोज़रों से/ कँपती थरथराती रही मैं। / तुम्हारे घरों की नींव / मेरी बाहों पर थी / अपने घर के मान में / सरो-सामान में / भूल गए तुम। / ... मैं थोड़ा हिली / तो लो / भरभराकर गिर गए / तुम्हारे घर। / फटा तो हृदय / मेरा ही।"
पर्यावरण ने सदा हमारे अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे पूर्वजों ने इसे भली -भांति समझा। विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो कर आज हम प्रकृति से दूर होते गए और परिणाम स्वरूप समय-समय पर हमने इसके दुष्परिणाम भी झेले हैं। पेड़ लगाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण वृक्षारोपण कर रहे हैं "तुलसी तरुवर विविध सुहाए/ कहुं कहुं सिया कहुं लखन लगाए।" यही नहीं जब राम वनवास से वापस आते हैं तब भी इस उपलक्ष्य में अयोध्या में वृक्षारोपण किया जाता है "सफल पूगफल कदलि रसाला। /रोपे बकुल कदम्ब तमाला।।" गोस्वामीजी ने यह भी लिखा कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग ही उचित है। पेड़ से फल तोड़ कर खाना तो उचित है लेकिन पेड़ को काटना अनुचित – “रीझि-खीझी गुरूदेव सिष सखा सुसाहित साधु।/ तोरि खाहु फल होई भलु तरु काटे अपराधू ।।"
पर्यावरण और इससे जुड़ी चिंताओं पर बहुत काम हुआ है लेकिन ज्यादातर काम वैज्ञानिक है। इस समस्या पर साहित्य में कम ही काम हुआ है और ऐसे में लेखिका के दोनों लेख महत्वपूर्ण हैं। एन्नी लेमोट (Annie Lamott) जो अमेरिका की प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ने एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी “ ‘No’ is a complete sentence.” यानि ‘नहीं’ एक सम्पूर्ण वाक्य है। सरकार ने धूम्रपान रोकने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, न जाने कितने बड़े-बड़े आलेख लिख कर इसके दुष्प्रभावों की चर्चा की गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिगरेट के डब्बे पर लिखा सिर्फ दो शब्द “Smoking Kills” या “धूम्रपान जानलेवा है” से ज्यादा प्रभावी कुछ भी साबित नहीं हुआ। ऐसे ही लेखिका के पर्यावरण पर दोनों लेख संक्षिप्त लेकिन बहुत ही प्रभावी है।
किताब का खंड दो ‘किन्नर विमर्श’ है जिसमें पाँच लेख संकलित हैं। ‘जो नर है न नारी’ शीर्षक लेख में लेखिका महेंद्र भीष्म द्वारा लिखे गए उपन्यास ‘किन्नर कथा’ और प्रदीप सौरभ के उपन्यास ‘तीसरी ताली’ की समीक्षात्मक आलोचना करते हुए किन्नरों की पीड़ा, उनकी पहचान, उनकी पूजा पद्धति आदि के बारे में विस्तृत विवरण देती हैं जो आम पाठकों के लिए रुचिकर और महत्वपूर्ण है। महेंद्र भीष्म के उपन्यास ‘किन्नर कथा’ की कहानी को लेखिका ने संक्षेप में लेकिन इतने प्रभावी ढंग से लिखा है कि पाठक इस कहानी का शब्द-चित्र अपनी आँखों के सामने बनता हुआ महसूस करेंगे।
“इक्कीसवीं सदी और किन्नर विमर्श” शीर्षक लेख में लेखिका ने नीरजा माधव कृत ‘यमदीप’, निर्मला भुराडिया कृत ‘गुलाम मंडी’, महेंद्र भीष्म कृत ‘किन्नर कथा’, प्रदीप सौरभ कृत ‘तीसरी ताली’ आदि किताबों के उद्धरण के साथ किन्नरों के साथ होने वाले भेद-भाव, सामाजिक अस्वीकार्यता, और रोजगार की समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए वांछित कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
“एक समांतर दुनिया: ‘तीसरी ताली’ ” शीर्षक लेख प्रदीप सौरभ के उपन्यास ‘तीसरी ताली’ की विस्तृत समीक्षा समेटे हुए है। प्रदीप सौरभ के लेखन की प्रशंसा में लेखिका लिखती है “लेखक ने छानबीन के बाद हिजड़ों की जीवन शैली, उनके बीच गद्दियों, इलाकों और गद्दी के वारिस को लेकर होने वाले खूनखराबे, किसी को जबरदस्ती हिजड़ा बनाने, चुनरी की रस्म, गुरु परंपरा का निर्वाह, मूंछों वाले गिरिया रखने, हिजड़ों के अंदर छिपी स्त्रीत्व की भावना, उनकी मानवीय संवेदना और ममत्व, हिजड़े होने के दर्द, उनके आक्रोश और संघर्ष आदि को विस्तार से परत-दर-परत खोला है। हिजड़ों के जीवन के साथ-साथ इस उपन्यास में एक समांतर दुनिया है समलैंगिकों की, विकृत प्रवृत्ति वालों की। इतना ही नहीं, लेखक ने राजनैतिक पैंतरेबाज़ी को भी उजागर किया है। उनकी मारक टिप्पणी देखिए – ‘असली हिजड़े तो वे हैं जो जनता के वोटों से संसद और विधानसभा में जाकर उन्हीं का खून चूसने की योजनाएँ बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं।’ ” किन्नर समुदाय अपनी स्थिति से किस कदर निराश है इसे लेखिका के इस कथन से समझा जा सकता है “दिल्ली में आमतौर पर हिजड़े के शव को रात को डंडों से मारते, उस पर चप्पल-जूते बरसाते और सड़क पर खींचते हुए श्मशान घाट ले जाते हैं। इस तरह शव को श्मशान में ले जाने के पीछे मान्यता है कि मरने वाला दोबारा तीसरी योनि में जन्म नहीं लेगा।” तीसरी ताली उपन्यास की समीक्षा के साथ ही लेखिका ने किन्नर होने के वैज्ञानिक कारणों पर भी प्रकाश डाला है। यहाँ लेखिका का विज्ञान की पृष्ठभूमि से होना सहायक सिद्ध होता है।
“सम्मान की ज़िंदगी जीने की चाहत : नाला सोपारा” शीर्षक लेख चित्रा मुद्गल के उपन्यास ‘पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा’ (2016) पर आधारित है जिसके लिए उन्हें 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है जिसमें एक पुत्र का बेबस माँ से संवाद है। उपन्यास में कुल मिलाकर सत्रह पत्र और उपसंहार में दो समाचार सम्मिलित हैं। उपन्यास के पात्र विनोद, जो एक किन्नर है, द्वारा लिखे गए पत्र इतने मार्मिक हैं जिसे पढ़ते समय पाठक भी अपने आप को विनोद के दर्द से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज-कल किसी भी विमर्श पर किसी भी लेखक द्वारा आनन-फ़ानन में कुछ लिख देने की परंपरा चल पड़ी है लेकिन ऐसे लेखों में विश्वसनीयता का अभाव झलकता है। यह उसी तरह है कि कोई लोहार, हलवाई को सुझाव दे कि अच्छे रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। किसी विमर्श पर लेख या तो स्वयं के अनुभव जनित होने चाहिए या उसे लेखक ने किसी और के माध्यम से इस तरह आत्मसात किया हो कि आप प्रभावी ढंग से उस विषय पर कुछ कह सकें। प्रो. ऋषभदेव शर्मा ने ‘देहरी’ शीर्षक से जो स्त्री-पक्षीय कविताएं लिखी हैं, उनमें स्त्रियों की पीड़ा इस तरह उभर कर सामने आती है जिसे शायद कोई स्त्री भी इस रूप में न लिख पाती। चित्रा मुद्गल भी इस उपन्यास में किन्नर की भावनाओं के इतने यथार्थ विवरण के पीछे के कारणों का उल्लेख करते हुए कहती हैं “जब मैं मुंबई के नाला सोपारा में रहती थी, तब मैं एक ऐसे ही युवक से मिली थी। उसे किन्नर होने की वजह से घर से निकाल दिया गया था। यह उपन्यास उसी युवक के विद्रोह की कहानी है। मैंने उसे अपने घर पर बहुत दिनों तक साथ रखा।”
“समसामयिक हिंदी साहित्य : किन्नर विमर्श” लेख, किन्नर विषय पर लिखे गए कई उपन्यासों, कहानियों और कविताओं के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह लेख लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की आत्मकथा ‘मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी’ (2015) की भी बात करता है जिसमें लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने अपने खुद के अनुभव के आधार पर किन्नर समुदाय के सच को उजागर किया है। यह देखना सुखद है कि साहित्यकारों का ध्यान किन्नर विमर्श की ओर गया है और इस दिशा में बहुत प्रयास हुए हैं लेकिन असली बदलाव तब होगा जब लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की ही तरह इसी समुदाय से और लेखक/लेखिका सामने आएं और अपने खुद के अनुभव और सत्य को सामने रखें।
स्त्री विमर्श खंड में छः लेख हैं। विमर्शों में सबसे ज्यादा शायद स्त्री विमर्श पर ही लिखा गया है लेकिन आज भी समस्या बनी हुई है। इन लेखों में लेखिका किसी किताब और किताब की समीक्षा के माध्यम से स्त्री विमर्श के विभिन्न आयामों को एक बार फिर से पाठकों के सामने लाती हैं और उम्मीद जताती हैं कि परिस्थितियाँ जल्द बदलें।
“कविता में स्त्री” शीर्षक लेख में लेखिका लिखती हैं ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी स्त्री को पग-पग पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। घर की दहलीज पार करके जहाँ स्त्री समाज में पुरुषों से कदम मिलाकर आगे चल रही है वहीं उसे जिल्ल्त भी उठानी पड़ रही है। प्रो. ऋषभदेव शर्मा की कविता ‘प्रशस्तियाँ’, स्त्रियों के इस दर्द को भली-भांति दर्शाती है - "मैंने जब भी कुछ पाया /मर खप कर पाया /खट खट कर पाया /अग्नि की धार पर गुज़र कर पाया /पाने की खुशी /लेकिन कभी नहीं पाई /***शिक्षा हो या व्यवसाय /प्रसिद्धि हो या पुरस्कार /हर बार उन्होंने यही कहा- /चर्म-मुद्रा चल गई! /[चर्म-चर्वणा से परे वे कभी गए ही नहीं!]”
“सनातन स्त्री : देह भी विदेह भी” शीर्षक से लेख में लेखिका ने दिनकर के काव्य उर्वशी के माध्यम से प्रेम की व्याख्या की है। “स्त्री-पुरुष की परस्पर-आश्रयता” शीर्षक से लेखिका यह स्थापित करती है कि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी या प्रतिबल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ‘अर्द्धनारीश्वर’ के देश में.... शीर्षक लेख में विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ‘अर्द्धनारीश्वर’ के बहाने लेखिका ने निर्भया और अन्य कई स्त्रियों के शारीरिक, मानसिक यातना और बलात्कार जैसी घटनाओं की चर्चा की है और न्याय मिलने में विलंब या न्याय न मिल पाने को इस समस्या की जड़ माना है। पुरुष प्रधान इस समाज में स्त्रियाँ या तो अपने साथ हुए अन्याय को बता ही नहीं पातीं और यदि बताया तो सामाजिक लांछन और न्याय न मिल पाने की वजह से ताउम्र बदनामी का दंश झेलने पर विवश होती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा “कामिहि नारि पिआरि जिमि” यह पुरुष प्रधान समाज की सोच को दर्शाता है। काम के अधीन औरत यदि सिर्फ प्यार की बात सोचती है तो काम के अधीन पुरुष क्या सोचता है? या पुरुष काम के अधीन होता ही नहीं? लेखिका ने इस सोच को बदले जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है “पुराने विधि-विधान और पुरानी स्मृतियाँ आज के संदर्भ में अर्थहीन हैं। आज नई स्मृतियों और नई संहिताओं की जरूरत है। सब कुछ बदलना होगा, सारे समाज की मानसिकता को बदलना होगा।”
“अल्पसंख्यक स्त्री का आधा गाँव “ शीर्षक लेख राही मासूम रज़ा कृत उपन्यास ‘आधा गाँव‘ पर आधारित है जो गंगौली गाँव के मुसलमानों का बेपर्द जीवन यथार्थ है। राही मासूम रज़ा ने गाँव के हिन्दू और मुस्लिमों के बीच पहले भाईचारे और उसके बाद बदलते हालात में आए परिवर्तन को बड़े ही प्रभावी ढंग से लिखा है। आम तौर पर स्त्री को फला की बेटी, फला की पत्नी, फला की माँ आदि कहकर संबोधित किया जाता है। उससे उसका नाम छीन लिया जाता है। इसी ओर इशारा करते हुए राही मासूम रज़ा ने ‘आधा गाँव‘ में कहा - ‘‘बेनाम होना तो बहुओं की तकदीर है। फ़र्क बस इतना हो जाता है कि अच्छे घरानों में वह या तो बहू कही जाती हैं या दुल्हन या दुलहिन। हमारे समाज में या तो यह होता है कि मैकेवाले दहेज देकर बेटी से अपना दिया हुआ नाम छीन लेते हैं या फिर यह कहिए कि ससुराल वाले इसे गवारा नहीं करते कि उनके यहाँ किसी और घर का दिया हुआ नाम चले। कभी-कभी यह बेनामी उन लड़कियों से ऐसी चिपक जाती है कि मरते-मरते पिंड नहीं छोड़ती।‘‘ इस संबंध में मुझे राजम पिल्लई की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है "गांधारी तुम्हारा नाम क्या है?" और गौर करने पर अचानक हम पाते हैं कि उस दौर में स्त्रियों के अपने नाम गुम हो गए। केकय देश की राजकुमारी केकई बन गईं तो कोशल देश की राजकुमारी कौशल्या। स्त्रियों को अपने नाम से भी अलग कर दिए जाने से ज्यादा अन्याय उनके साथ और क्या होगा। राही मासूम रज़ा झंगोटिया-बो और सईदा दो पात्रों के बारे में लिखते हैं जिन्हें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपने शरीर से समझौता करना पड़ा। नीरजा लिखती हैं "सर्वत्र शरीर संबंध है और इस संबंध के पीछे सवाल आर्थिक हैं। परदे के भीतर भी स्त्री का संघर्ष और उसका आत्मसंघर्ष चलता रहता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी चल रहा है।"
लघुकथा विमर्श खंड में लेखिका ने श्याम सुंदर अग्रवाल, कमल चोपड़ा और सीमा सिंह की लघुकथाओं का विस्तृत विश्लेषण और विवेचन किया है। लेखिका का कहना है कि आज की लघुकथाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विसंगतियों को लघुकथाकारों ने अपना कथ्य बनाया है। लघुकथा आंदोलन से जुड़कर अनेक साहित्यकारों एवं पत्र-पत्रिकाओं ने इस विधा को सशक्त बनाया। विष्णु प्रभाकर ने अपने लघुकथा संग्रह ‘आपकी कृपा है’ की भूमिका में लिखा कि “विकास की एक सुनिश्चित परंपरा आज की लघुकथा के पीछे देखी जा सकती है। न जाने किस काल-खंड में मनीषियों ने अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत देने की आवश्यकता अनुभव की, इसी अनजाने क्षण में लघुकथा का बीजारोपण हुआ। तब उसका नाम दृष्टांत या ऐसा ही कुछ रहा होगा।” लेखिका ने कहा है कि 1901 में ‘छत्तीसगढ़ मित्र’ में प्रकाशित माधवराव सप्रे की रचना ‘एक टोकरी भर मिट्टी’ को हिंदी की पहली लघुकथा माना जाता है।
श्याम सुंदर अग्रवाल की कई लघु कथाओं का विश्लेषण करते हुए लेखिका ने उनकी लघुकथाओं में सामाजिक कुरीति पर प्रहार, व्यवस्था पर व्यंग्य, गरीबी आदि को तो रेखांकित किया ही है, वैज्ञानिक समालोचना करते हुए लघु कथा शिल्प, कथाओं में संवाद, विवरण, निपातों का प्रयोग, स्थानीय भाषा प्रयोग, विस्मयादिबोधक/ प्रश्न चिन्ह/ पुनरावृति/ अल्पविराम आदि के प्रयोगों को उदाहरण के साथ पाठकों के सम्मुख रखा है जो पाठकों को लघु कथा के स्वरूप, औचित्य, शिल्प और महत्व को समझने में सहायक सिद्ध होगी। श्याम सुंदर अग्रवाल की लघु कथाओं के बारे में लेखिका ने लिखा है “श्याम सुंदर अग्रवाल अपनी लघुकथाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त मूल्यहीनता, मानवाधिकारों के हनन और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व नैतिक विडंबनाओं पर सीधे-सीधे प्रहार करते हैं। गरीबी और भूख के अमानुषिक सच को उन्होंने इस तरह उकेरा है कि व्यंजनापूर्ण शब्दावली पाठक के हृदय को छील देती है। वे सरल संप्रेषणीय भाषा प्रयोग द्वारा भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य कसते ही हैं अनेक लघुकथाओं के अंत में झिड़की भी देते हैं।“
कमल चोपड़ा के लघुकथाओं का भी नीरजा साहित्यिक और वैज्ञानिक विश्लेषण तो करती ही हैं, साथ ही लघु-कथा के बारे में कई साहित्यकारों के कथन के माध्यम से लघु कथा की परिभाषा और लघु कथा के महत्व को स्थापित करती हैं। कमल चोपड़ा की लघु कथाओं में अच्छी कथा होने के सभी अवयव होने की बात करते हुए लेखिका लिखती हैं “अपनी लघुकथाओं में कमल चोपड़ा सामाजिक विसंगतियों पर सीधा प्रहार करते हैं और कथा के अंत में ‘पंच’ के साथ उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। इनकी भाषा बोधगम्य तथा परिवेश और पात्र के अनुरूप है। इनकी लघुकथाओं में व्यंग्य भी है और फटकार भी; आक्रोश भी है और चेतना तथा जागरूकता भी।“ सीमा सिंह की लघु कथाओं के बारे में लेखिका का यह कथन द्रष्टव्य है “सीमा सिंह ने स्त्री जीवन के विविध पक्षों पर लेखनी चलाई है। सरल, सहज और संप्रेषणीय भाषिक प्रयोग से स्त्री-प्रश्नों को उकेरा है और साथ ही उनका निदान किया है। वे सड़ी-गली मान्यताओं को तोड़ कर नवीन जीवन मूल्यों को स्थापित करने में विश्वास रखती हैं और यह आशा करती हैं कि स्त्री को खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो।"
“विमर्श विविधा” इस किताब का पाँचवां और आखिरी खंड है जिसमें अलग-अलग विमर्शों के आठ लेख संकलित हैं। डॉ. रमेशचंद्र शाह को उनके उपन्यास ‘विनायक’ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाने की बात से आरंभ करते हुए “सृजन के आयाम : रमेशचंद्र शाह” शीर्षक से लेख में नीरजा ने लेख के पहले भाग में डॉ. रमेश चंद्र शाह का परिचय और उनके साहित्य का परिचय दिया है, भाग दो में लेखिका के डॉ. रमेश चंद्र से मुलाकात से संस्मरण है जिनमें लेखिका के प्रति डॉ. रमेश चंद्र शाह का कथन दक्षिण भारत में हिंदी की सेवा में लगे साहित्यकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है “मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हमेशा यही कहता हूँ कि हिंदी का उद्धार दक्षिण भारतीय ही करते हैं और वे ही यह काम कर सकते हैं। क्योंकि वे अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।” इसी लेख में लेखिका ने साहित्यकार डॉ. रमेश चंद्र की एक आलोचक के तौर पर, एक कवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में मीमांसा की है। उनके उपन्यास ‘विनायक’ के माध्यम से लेखिका ने उनके गद्य लेखन पर भी विस्तृत चर्चा की है।
“समाज विमर्श : रमेश पोखरियाल ‘निशंक’” शीर्षक से लेखिका ने डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में परिचय देते हुए उनकी कविताओं और कहानियों के माध्यम से परिवार और समाज के प्रति उनके विचारों को सामने रखा है। डॉ. निशंक ने खुद कहा है कि एक राजनेता होने से पहले वे साहित्यकार और समाजसेवी हैं। लेखिका ने लिखा है “रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की दृष्टि सुधारवादी है। वे मनुष्यता को कायम रखने की बात करते हैं। उनकी कहानियों में आदर्श की स्थिति को देखा जा सकता है। वे यथार्थ की परिस्थितियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें सोचने के लिए बाध्य करते हैं और उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए राह भी सुझाते हैं। वे मानवीय मूल्यों एवं आदर्श परिवार को प्रमुखता देते हैं।”
वरिष्ठ हिंदी कवि केदारनाथ सिंह को सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार (2013) से सम्मानित किए जाने के संदर्भ में “लोकतंत्र और लोक विमर्श : केदारनाथ सिंह” शीर्षक से लेख में लेखिका ने केदारनाथ सिंह की कविताओं में ज़मीन से जुड़ाव और मिट्टी की खुशबू की बात की है। लेखिका ने लिखा है कि केदारनाथ सिंह की कविताओं में गाँव की प्राकृतिक आभा की अनेक छवियाँ दिखाई देती हैं। इनकी कविताओं के बिंब में नदी, नाले, फूल, जंगल, तट धूप, सरसों के खेत, धानों के बच्चे, बन, सांध्यतारा, बसंत, फागुनी हवा, पकड़ी के पात, कोयल की कूक, पुरवा-पछुवा हवा, शरद प्रात, हेमंती रात, चिड़िया, घास, फुनगी आदि बार-बार आते हैं जो इनके मिट्टी से जुड़ाव का परिचायक है। बिंब के बारे में केदारनाथ सिंह का कथन महत्वपूर्ण है “बिंब पाठक को रोकता-टोकता चलता है और एक हद तक उसे विवश करता है कि वह रुके और सोचे और समग्र कविता के बारे में तुरत-फुरत कोई फैसला न दे। यह रचनात्मक बाधा शायद एक ऐसी कसौटी है जिस पर हम कविता का श्रेणी विभाजन कर सकते हैं।”
“समकालीन कविता : उत्तरआधुनिक विमर्श” शीर्षक लेख में लेखिका ने संप्रेषणीयता को कविता की मुख्य चुनौती माना है। आज की नई पीढ़ी जिनकी पहुँच विश्व साहित्य तक है और इंटरनेट के माध्यम से विश्व घर जैसा है, की कविताओं के बिंब वैश्विक परिदृश्य से प्रभावित हैं। लेखिका ने कुमार लव की कविता का उल्लेख किया है “प्रोमेथ्यूज़ का कलेजा/ हर रोज़ नोचती चील/ सोचती होगी/ कैसा मूर्ख है यह,/ देवताओं से लड़ता है भला कोई!!” यहाँ प्रोमेथ्यूज़ के बारे में जाने बिना इस बिंब को समझा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वह पीढ़ी है जो आज भी गाँव को याद करते हुए अपने को उस मिट्टी से जुड़ा हुआ पाती है और उनकी कविताओं के बिंब में यह भाव आयातित होता है। लेखिका ने प्रो. ऋषभदेव शर्मा की कविता का उल्लेख किया है “चिकनी पीली मिटटी को/ कुएँ के मीठे पानी में गूँथकर/ बनाया था माँ ने वह चूल्हा/ और पूरे पंद्रह दिन तक/ तपाया था जेठ की धूप में/ दिन दिन भर/ उस दिन/ आषाढ़ का पहला दौंगड़ा गिरा,/ हमारे घर का बगड़/ बूंदों में नहा कर महक उठा,/ रसोई भी महक उठी थी –/ नए चूल्हे पर खाना जो बन रहा था।/ गाय के गोबर में/ गेहूँ का भुस गूँथ कर/ उपले थापती थी माँ बड़े मनोयोग से/ और आषाढ़ के पहले/ बिटौड़े में सजाती थी उन्हें/ बड़ी सावधानी से।” आज की युवा पीढ़ी अपने आप को इन कविताओं से तारतम्य बिठाने में सहज नहीं पाती। डॉ. नीरजा ने हालांकि यह नहीं लिखा कि प्रो. ऋषभदेव शर्मा और कुमार लव पिता-पुत्र हैं लेकिन फिर भी यह न सिर्फ कविता के स्तर पर बल्कि दो पीढ़ियों के बीच आपसी संवाद के स्तर पर भी संप्रेषणीयता के संकट को दर्शाती है। दो चुंबक के ध्रुव जब समान दिशा में हों तो उनमें विकर्षण होता है। कविता और वर्तमान पीढ़ी दोनों ही इस विकर्षण के दौर से गुजर रही है जहाँ संप्रेषणीयता एक बड़ी समस्या है। अगली पीढ़ी तक आते-आते जब दोनों ही पीढ़ी के लोग वैश्विक समझ रखने वाले होंगे तब शायद चुंबक के दोनों ध्रुव आसमान दिशा में हों जाएं और यह दूरी मिट जाए । ‘वक्तव्य प्रधानता’ और ‘अभिव्यक्ति का खतरा’ को लेखिका ने कविता की अन्य चुनौतियों में शामिल किया है।
“नई सदी की कविता का दलित परिप्रेक्ष्य” शीर्षक लेख में लेखिका विभिन्न कविताओं के माध्यम से दलित विमर्श पर चर्चा करती हैं तो “विस्थापन विमर्श : भाषा की आजादी” शीर्षक लेख से महुआ माजी के उपन्यास 'मैं बोरिशाइल्ला' की समीक्षा करते हुए लेखिका ने विस्थापन के दर्द को उकेरा है। “संताल संस्कृति की संघर्ष महागाथा : बाजत अनहद ढ़ोल” शीर्षक लेख संताल आदिवासियों के संघर्ष को याद करते हुए उनकी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास है। किताब का आखिरी लेख “वृद्धावस्था विमर्श” है। जिस तरह जीवन का आखिरी पड़ाव वृद्धावस्था है वैसे ही सभी विमर्शों की चर्चा के बाद लेखिका ने वृद्धावस्था विमर्श की बात की है, हालांकि यह last but not the least है। इस महत्वपूर्ण विमर्श में वृद्ध लोगों के साथ स्नेह और सद्भाव बनाए रखने के आह्वान के साथ लेखिका लिखती हैं “वास्तव में वृद्धों को चाहिए थोड़ा सा स्नेह और आत्मीयता। उन्हें आश्वासन चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। बस यही उनकी अपेक्षाएँ हैं।” और इतना तो हम उन्हें दे ही सकते हैं।
जी. नीरजा के इन लेखों को पढ़ते हुए अनायास ही मेरे ज़ेहन में बचपन में की गई रेल यात्रा उभरती है जिसमें खट्टी-मीठी चौकलेट बेचने वाला ‘बारह मसाले तेरह स्वाद’ की आवाज़ लगाता था। ये सभी लेख अलग-अलग समय में लिखे गए हैं इसलिए इनकी अपनी अलग पहचान तो है ही लेकिन इस किताब में संकलित हो जाने और इन्हें एक साथ पढ़ने से पाठक इन लेखों के ‘तेरहवें स्वाद’ से भी परिचित हो सकेंगे। जी. नीरजा अपने लेखों में, स्थापित किताबों के माध्यम से मजबूत तटबंध बनाती हैं और फिर इन तटबंधों के बीच अपनी बात प्रखरता से रखती हैं इस बात से आश्वस्त कि ये तटबंध उन्हें विषयांतर से बचाते हुए अपनी बात रखने की आज़ादी देंगे। लेखिका के शब्दों की सरलता सुनिश्चित करती है कि इन तटबंधों के बीच इनके विचारों का प्रवाह अवरुद्ध न हो। हालांकि यह किताब आधुनिक साहित्य की बात करती है लेकिन इसमें संकलित कई विमर्श हमें इस परिधि से परे देखने का आग्रह करते हैं। अज्ञेय ने भी लिखा “आधुनिक हिंदी साहित्य की परंपरा अथवा उसका परिदृश्य उतना लंबा नहीं है कि कुछ बातों की परीक्षा हम उसी की सीमा के भीतर रहते हुए कर सकें। लेकिन यह बिल्कुल जरूरी भी नहीं है, उचित भी नहीं है, कि हम अपने को उसी सीमा से बांध कर रखें।“ मितभाषी नीरजा, जो बहुत ही कम बोलती हैं, के आसपास शब्दों का सन्नाटा रहता है लेकिन उनके लिखे शब्द राष्ट्रीय परिदृश्य पर कोलाहल मचा रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कोलाहल थमेगा भी नहीं।